Radhika : Krisha : Darshan Alekh Arun Kumar
©️®️M.S.Media.
Shakti Project.
कृण्वन्तो विश्वमार्यम.
In association with.
A & M Media.
Pratham Media.
Times Media.
Presentation.
---------------------
आवरण : पृष्ठ.
*
शक्ति.आरती*
---------
सम्पादकीय आलेख :१ / ३
-------------
⭐
प्रथम मीडिया शक्ति *समर्थित.
--------
आस्था, श्रद्धा, विश्वास,भक्ति और प्रेम : शक्ति. आलेख : १ /३ /८
--------
आलेख : अरुण कुमार सिन्हा : शक्ति. आरती.
प्रेम स्वत: स्फूर्त होता है : ये ऐसे विषय और ऐसी अनुभूतियां हैं जिसके प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती,ये स्वत: स्फूर्त प्रदर्शित होते रहते हैं जैसे सूर्य को स्वयं प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं सिद्ध है।
यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर किसी को प्रेम करते हैं तो दिखना चाहिए,क्या हनुमान ने कभी घोषणा की कि वह श्री राम से प्रेम करते हैं, क्या मीरा,राधा, गोपियों और उद्धव चैतन्य महाप्रभु ने कभी कहा कि वे श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं ? क्या कभी कोई कभी अपने बच्चों से कभी कहती हैं कि मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करती हूॅं ?
अपनों के लिए भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति ही प्रेम है : है ना ? नहीं न ! पर सांसारिक जीवन प्रश्न चिह्न खड़ा करता रहता है कि प्रेम दिखना चाहिए तो हमने कहा ही कि इसका प्रदर्शन स्वत: स्फूर्त होता रहता है और यह भावों की गहराईयों को भी बताते रहता है। अब यहां एक द्वन्द्व पैदा होता है कि कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेम का स्वरूप क्या है कि प्रेम मूलतः प्रेम ही है पर सौर रश्मियों की तरह उसके रंग अलग-अलग होते हैं पर वो रहता प्रेम ही है।
पर संसार में प्रेम की अभिव्यक्ति लोग देखना चाहते हैं जो भौतिक रुपों में की जाती है जो संसाधनों और समर्पण के एक सम्मिलित रुप में समय समय पर प्रदर्शित होते रहते हैं।
भावनाओं की अभिव्यक्ति कभी छुपती नहीं,वैसे ही प्रेम कभी छुपता नहीं तो फिर प्रदर्शन की क्या जरूरत है, कविवर रहीम जी कह ही गए हैं,
खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मधुपान
छिपाए से भी ना छिपे कह गए रहीम सुजान
तो चीजें छिप नहीं सकती उनके प्रदर्शन की फिर क्या जरूरत है पर तथ्य आस्था श्रद्धा विश्वास और भक्ति में बड़ा द्वन्द्वात्मक सा प्रतीत होता है,जो जितने भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए कर्मकाण्ड के प्रदर्शन में लगे रहते हैं उनके इष्ट उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते हैं पर ऐसा भी पूर्ण सत्य नहीं है। परन्तु भक्ति आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ हो तो स्वीकार्य है अन्यथा याचना सुरक्षा और प्रदर्शन ही है।इसे एक बड़े रोचक प्रसंग से बताने की कोशिश करता हूॅं।
एक पूजारी और एक मौलवी :किसी गांव में दो दोस्त रहते थे जिनमें एक पूजारी और एक मौलवी थे जो दिन रात अपने अपने पांथिक कर्मकांड का निष्पादन किया करते थे। मौलवी साहब हाजी भी थे, पांचों वक्त के नमाज़ी और नियमित रोजा भी रखते थे। मस्जिद में अपनी तकरीर भी किया करते थे।
इधर पूजारी जी भी त्रिसंध्या करते,हर व्रत त्योहार में उपवास करते, निश्चित समयों पर मंदिर में घंटा और शंख भी बजाया करते। यही नहीं अपने मित्र की तरह चारों धामों और सारे तीर्थों की परिक्रमा भी कर चुके थे। संयोगवश उन दोनों की मौत एक ही दिन और एक ही समय हो गया। दोनों की ये समझ थी कि हम तो बड़े पूण्यात्मा रहे हैं, हमें तो स्वर्ग या जन्नत ही मिलेगा।
दोनों एक साथ वहां पहुंचे तो स्वर्ग और नर्क के दरवाजे अगल-बगल ही थे। दोनों दरवाजों पर देवदूत या फ़रिश्ते खड़े थे। वे बगैर कुछ कहे सुने सीधे स्वर्ग में घुसने लगे तो उनको रोक लिया गया। उन्होंने द्वारपालों से कहा कि हमदोनों तो जीवन भर अपने अपने इष्ट की पूजा उपासना इबादत की है, हमनें हज किया है,सारे धामों और तीर्थ स्थलों की यात्राए भी की है, तो हम तो सीधे स्वर्ग में ही जाएंगे, जन्नत ही अब हमारा आश्रय है।
तब दोनों को बताया गया कि आप दोनों ने सिर्फ आडंबर और पाखंड किया है। मौलवी साहब रोज़े में भी दिनभर बढ़िया बढ़िया खाने पर नजर रखते थे, इफ्तार पर सारा जेहन रहता था और आप भी उपवास में ऐसा ही किया करते थे कि कब शाम हो और मेवा मिष्ठान खाया जाए जबकि उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं अपने इष्ट के सान्निध्य में रहकर ध्यान करना है।
आप शंख और घंटे पब्लिक को आकर्षित करने और दक्षिणा लेने पर ध्यान रखते थे। तीर्थाटन के नाम पर सीधे सरल लोगों से पैसा ठगकर आपने अपना घर बनवा लिया और बाकी कर्म आपने जीविकोपार्जन का साधन बना लिया।
आस्था,श्रद्धा, विश्वास और भक्ति : आपके पूजा पाठ आपकी आस्था,श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से कोसों दूर थे और यही काम आपके दोस्त मौलवी साहब ने किया कि चंदा उठाकर हज कर आए और हाजी होने के नाम पर झगड़ों का ग़लत फैसला करके कमाई का जरिया बना लिया।
नमाज़ और रोज़ा इनका फरेब था,उनके आड़ में ये सारे गलत काम करते थे, इसलिए आप दोनों को माफी नहीं मिलेगी। आप दोनों नर्क या दोजख में जाकर प्रायश्चित और पश्चाताप करें और अपने अपने इष्ट की सच्ची आराधना करें फिर आप दोनों पर विचार किया जाएगा और यह कहकर उन दोनों को नर्क में धकेल दिया गया।
इस कथा का यह अंत नहीं है और यह संदेश देना भी नहीं है कि आप अपने मत,पंथ, विश्वास आदि में मान्य
परम्परागत पूजा पाठ न करें,जरुर करें पर स्वयं को, लोगों को और अपने अपने भगवान को परमात्मा को धोखा न दें।
साक्षी आप स्वयं : सबसे बड़ी गवाही या साक्षी आप स्वयं होते हैं जिसे आत्मसाक्षी कहा जाता है। आत्मसाक्षी ही परमात्मा की साक्षी है। परमात्मा स्थूल रुप में नहीं देखते पर आप अपने हर कर्म को स्वयं साक्षी बनकर देखते और करते हैं, परमात्मा सूक्ष्म साक्षी भाव में रहते हैं इसलिए आस्था, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति आपके निज की चेतना और बोध है।मन, चित्त,हृदय और आत्मा की शुद्धता और अपने प्रति और सबके प्रति विहीत कर्मों अर्थात् कर्तव्यों का निर्वहन ही श्रेष्ठ पूजा है,यही सच्ची आराधना, उपासना और इबादत है। व्रत त्योहार आदि मन को उनके प्रति निष्ठा और समर्पण का एक माध्यम है तो उनमें दिखावा, प्रदर्शन और आडम्बर नहीं होना चाहिए। दूसरों का धन आदि हड़पकर दान और तीर्थाटन करने से क्या लाभ होगा, दूसरों का दिल दुखाकर उपवास करने के क्या लाभ होंगे कि जो आपके व्यवहार आचरण आदि से पीड़ित होंगे उनके भीतर से आह और हाय निकलेगी जो आपके सुख चैन को छीन लेगी। यह सच्चा हज और तीर्थाटन और चारों धाम की यात्रा नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा भी है,
तुलसी आह गरीब के कबहुं न निष्फल जाए
मुआ खाल के चाम से लौह भस्म हो जाए।
इसलिए अगर सबकी दुआएं न ले सकें तो बद्दुआओं से भी बचिए। साफ रहिए और वही दिखने की कोशिश कीजिए जो आप हैं कि एक दिन तो सबकी किताब पढ़ी ही जानी है और जब आपकी किताब पढ़ी जाएगी तो उस मूल्यांकन का कोई काट नहीं होगा।
----------
प्रेम : जहां श्रेष्ठता या अहंकार का भाव नहीं हो : शक्ति.आलेख : १ / ३ / ७ .
----------
आलेख : शक्ति.आरती.अरुण.
*
प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय.
प्रेम बहता हुआ जल प्रवाह अर्थात् नदी या जलप्रपात है जो किसी कारण बाधित हो गया तो स्थिर जलाशय में रुपान्तरित हो जाता है। इसलिए प्रेम में सातत्य का होना एक जरुरत है। हम सब जीवन में एक दूसरे से जरूरत, जज्बात और पारस्परिक समझ के आधार पर प्रेम करते रहते हैं। और उन तीनों का सातत्य उस प्रेम को जीवित रखने का काम करता है जिसके बीच हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि सम्मान भी प्रेम से ही जुड़ा रहता है।
प्रेम के लिए सबकुछ स्वीकार्य है पर श्रेष्ठता और अहंकार का बोध प्रेम रुपी वृक्ष का दीमक है जो बाहर से तो दिखाई नहीं पड़ता पर भीतर ही भीतर वह खोखला करता जाता है और एक दिन वृक्ष की तरह नष्ट हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने तो कह ही दिया है.
प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय
राजा परजा जे रुचे सीस दिए ले जाए,
अर्थात् प्रेम सबके लिए सुलभ है, वह हाट बाजार में बिकने वाला सामान नहीं जिसकी कीमत देकर क्रय विक्रय किया जाए। यह जो धनी निर्धन सबके लिए सुलभ है परन्तु एक शर्त है कि सहज भाव से एक दूसरे के प्रति समर्पण करना होगा, जहां श्रेष्ठता या अहंकार का भाव नहीं होगा, वही कबीर जी ने कहा है कि प्रेम के लिए सीस अर्थात् अहंकार देना होगा, स्वयं को समर्पित कर देना होगा, द्वैत को अद्वैत में रुपान्तरित करना होगा और तभी प्रेम अपने आकार को ग्रहण कर सकेगा अन्यथा वह प्रेम नहीं होगा बल्कि मोह, चाहत, जरुरत और आकर्षण होकर रह जाएगा।
प्रेम के प्रवाह में सम्पूर्ण प्रकृति बहती नजर आती है,आप सुबह-शाम इसका अवलोकन कर सकते हैं,सब प्रेम के आश्रय में जाने के लिए व्याकुल रहते हैं और व्याकुलता ही प्रेम का शाश्वत गुण है। पीड़ा,विरहानुभूति,
वेदना, प्रतीक्षा आदि प्रेम के गुण हैं और जो इनकी अनुभूति करते हैं,वही प्रेम के रहस्य को समझ सकते हैं।
सती के लिए शिव का विलाप, जानकी के विरह में राम का विलाप, कृष्ण के लिए राधा,मीरा और गोपियों का विलाप, हीर के लिए रांझा का और लैला के लिए मजनूं का विलाप,कुछ ऐसे ही अलौकिक और लौकिक उदाहरण हैं जिसे समझने के लिए गहराईयों में डूबना पड़ता है जैसे सागर की अतल वितल गहराईयों में डूबे बगैर रत्न नहीं मिलते, वैसे ही प्रेम रुपी रत्न की प्राप्ति के लिए भावों की गहराईयों में डूबना पड़ता है,बाकी सब माया मोह है।
--------
बुद्ध : शक्ति * आलेख : दुःख है, दुःख का कारण भी है : पृष्ठ : १ / ३ / ६ .
---------
आलेख : अरूण कुमार सिन्हा.
शक्ति.आरती.
हरि के कल्कि अवतार : गौतम बुद्ध
अहिंसा परमो धर्मः
इसका निवारण भी है : मध्यम मार्ग : अष्टांगिक मार्ग.
सम्यक साथ : सम्यक दृष्टि : सम्यक कर्म
धर्म-कर्म सुधार आन्दोलन : भगवान बुद्ध की महिमा कुछ ऐसी थी कि इन्हें एशिया का प्रकाश तक कहा गया आजीवक ( चार्वाक ) सम्प्रदाय, जैन मत और बौद्ध मत को तत्कालीन भारत में भारतीय सामाजिक आर्थिक, धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधारभूत संरचनाओं में एक मौलिक बदलाव के रुप में इनको देखा गया और इसलिए इतिहासकारों का एक वर्ग इसे धर्म-कर्म सुधार आन्दोलन भी बताया है।
It was not the emergence of any faith belief or dogma based on the concept of Dharma but a new way and methodologies of life which was the need and demand of the time.
इस सन्दर्भ में भगवान बुद्ध ने अपनी धम्मदेसना में स्वयं कहा है कि, मैं किसी नवीन धर्म या मत सम्प्रदाय की बात नहीं कर रहा हूॅं पर स्थापित जीवन मोल और मूल्यों में परिवर्तन की बात कर रहा हूॅं जिससे जीवन परिष्कृत मर्यादित और चैतन्य हो और मनुष्य जीवन के अर्थों को समझ सके।
तथागत सिद्धार्थ : सुजाता : सम्बोधि : तथागत सिद्धार्थ ने इसीलिए वैदिक और वेदान्त दर्शन का भी अध्ययन चिन्तन और मनन किया और इसके लिए वे अनेक सिद्ध विद्वानों के पास जाकर ज्ञान भी हासिल की। उनके पहले गुरु आलार कलाम थे। परन्तु इन्हें कहीं भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, प्यास नहीं बुझी और ये भटकते भटकते निरंजना नदी के किनारे आज का बोधगया पहुंच कर साधनारत हो गए पर वहां भी इन्हें वह न मिला जिसकी खोज थी। जब ये खोज की अति पर पहुंच गए तो सुजाता के गीत सुनकर और उसके हाथों खीर खाकर इनकी चेतना का विस्फोट हुआ जिससे सम्बोधि की प्राप्ति हुयी और सिद्धार्थ एक निमिष में मानव से महामानव बन गए। 'बुद्ध ' को आमतौर पर लोग एक नाम समझते हैं पर ' बुद्ध ' तो एक संज्ञा नहीं ' विशेषण है। ' बुद्ध ' होना एक ' चैतन्य अवस्था ' है और इस अवस्था की प्राप्ति स्वयं के श्रेष्ठ कर्म और गुण जनित संस्कारों से की जा सकती है। गौतम सिद्धार्थ के पूर्व भी कई ' बुद्ध ' हुए हैं जो विभिन्न कालखंडो में विभिन्न प्रदेशों में अवतरित जन्म के अर्थ में हुए हैं।
जीवन में दुःख है,
दुःख के कारण हैं,
उनके निदान हैं
और निदान के मार्ग हैं अष्टांगिक मार्ग
अहिंसा, करुणा क्षमा, प्रेम और त्याग : तथागत सिद्धार्थ के अहिंसा, करुणा क्षमा, प्रेम और त्याग की प्रेरणा के साथ साथ प्रचलित याज्ञिक कर्मकाण्ड के विरोध और जीवन को नवीन रुप में परिभाषित करने के कारण उनका मत और विचार चतुर्दिक विस्तारित हो गया और तत्कालीन भारतीय आमजन समाज में स्थापित हो गया।
लोग बलि, हत्या,यज्ञ हिंसा और अन्य कर्मकाण्डों से उबे हुए थे जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध मत ग्राह्य हो गया। ऐसे उनके जितने दर्शन और चिन्तन हैं, महत्वपूर्ण और व्यवहार के योग्य हैं परन्तु एक दर्शन ने सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थान को पाया वह ' पटिच्चसमुप्पाद् ' है जिसे संस्कृत में ' प्रतीत्यसमुत्पाद ' कहा गया है। इसका सीधा सादा मतलब ' कार्य और कारण का सिद्धान्त ' हैं।
अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन और चिंतन से इस सिद्धान्त का क्या लेना देना है। लेना देना तो यह है कि यह सम्पूर्ण बौद्ध धर्म और दर्शन के मूल में रीढ़ की हड्डी की तरह है, कहा जाता है कि इस दर्शन और चिंतन के बगैर सिद्धार्थ कभी तथागत बुद्ध नहीं हो सकते थे। शब्दार्थ के बाद इसके कार्यभेद को भी जानना जरूरी हो जाता है।
इसकी व्याख्या करते हुए एक पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि ' this law establishes the fact of the existence of any thing whether it is living or non living whether it is an object Or incident then there must be a set of causes or reasonable reasons behind it '
अनात्मवाद और अनिश्वरवाद : अर्थात् किसी का होना अगर उद्देश्यपूर्ण है तो निश्चय ही उसका कोई कारण होगा, 'प्रतीत्य' ( कारण ) है तो ' समुत्पाद ' उसका उत्पाद या परिणाम अवश्य होगा। सिद्धार्थ ने इसी नियम के आधार पर अपने ' धर्म दर्शन और चिंतन को विकसित किया और ' अनात्मवाद और अनिश्वरवाद ' की व्याख्या की और बताया कि समस्त ब्रह्माण्डीय क्रियाशीलताओं का आधार कारण और कार्य का सिद्धान्त है जो स्वत: स्फूर्त क्रियाशील है जिसके पीछे कोई अलौकिक सत्ता का अस्तित्व नहीं हैं।
यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अगर बुद्ध किसी बाह्य सत्ता की बात करते तो उन्हें आत्मा परमात्मा और अन्य सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता और जिस बदलाव को वह लाना चाह रहे थे, नहीं आता और कोई परिवर्तन नहीं हो पाता और यही कारण है कि उन्होंने ईश्वरीय सत्ता और इससे सम्बन्धित बारह सवालों के कोई जवाब नहीं दिए और ऐसे प्रश्न किए जाने पर या तो मौन हो जाते या उन प्रश्नों को अव्याकृत कहकर अस्वीकार कर देते।
कर्म की श्रेष्ठता : कर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए कर्म जनित श्रेष्ठता से उत्पन्न संस्कारों के द्वारा मोक्ष की जगह ' निर्वाण और महापरिनिर्वाण ' की बात की। मूलतः यह सिद्धान्त ' औपनिषदिक दर्शन और चिंतन में स्थापित ' कर्मवाद के सिद्धान्त ' से अभिप्रेरित और अनुप्राणित है जिसकी व्याख्या तथागत सिद्धार्थ ने अपने तरीके से की। यही सिद्धान्त विज्ञानवाद भी कहलाता है जिससे प्रकृति के सारे क्रियाकलापों की व्याख्या की जाती है।
इस कालखंड के बड़े भौतिकविद् आईजक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त और न जाने कितने आधुनिक सिद्धान्त इसी पर आधारित है। सम्प्रति संसार की जो अवस्था है और हम मनुष्य जिस संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, क्या यह बताने की जरूरत है कि हमें ' किसी भी क्रियाशीलता की अति से बचना ' चाहिए। या तो हमने इस प्रकृति के साथ अति किया है या विज्ञान के साथ अति अर्थात् विज्ञान को विकृत करने का काम करने का काम किया है।
इस तरह अगर ' प्रतीत्य ' हम हैं तो त्रिविध ताप संकट इसका ' समुत्पाद ' है और यही परिदृश्य उस सिद्धान्त की प्रासंगिकता को सही सिद्ध करता है। हमने इसी आलेखों के माध्यम से कितनी बार कहा है कि सत्य का जो हिस्सा निरपेक्ष मूल्यों पर आधारित है वही टिकेगा शेष कालप्रवाह में बह जाएगा।
अब आज की वैश्विक व्यवस्था में अहिंसा, क्षमा, दया, करुणा, त्याग आदि की कितनी जरूरत और प्रासंगिकता है, विश्लेषण का विषय है। उनके सारे दर्शन और चिन्तन आज भी व्यवहारिक और ग्राह्य हैं बस बहस हिंसा और अहिंसा के उपर है। प्रेम, क्षमा ,दया , त्याग और करुणा सार्वकालिक और सार्वभौमिक है पर अहिंसा और हिंसा को नये सन्दर्भों में देखने की जरूरत है।
अहिंसा परमो धर्म : जिस कालखण्ड में तथागत सिद्धार्थ ने अहिंसा परमो धर्म की बात की थी,वह कुछ और था और आज की वैश्विक व्यवस्था कुछ और है। कोई भी दर्शन और चिन्तन में सामयिक जीवन मोल और मूल्यों के रक्षा के आधार होने चाहिए अन्यथा वह मूल्यहीन हो जाता है। रक्षा करने का सामर्थ्य सिर्फ शक्तिशाली में ही हो सकता है, निर्बल न तो स्वयं की रक्षा कर सकता है न औरों की रक्षा कर सकता है। कहा भी गया है कि ,समरथ को नहीं दोष गुसाईं अर्थात् जो शक्तिशाली और सामर्थ्यवान हैं वे कभी दोषी नहीं ठहराए जाते हैं। भय नाग से किया जाता है,जलसर्प से कोई नहीं भयाक्रांत होता है। दिनकर जी ने भी कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसलिए अहिंसा जैसे सद्गुण की रक्षा तभी हो सकती है जब बुद्ध के पीछे कृष्ण हों अन्यथा अहिंसा की महत्ता समाप्त हो जाएगी। भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता कल भी थी और कल भी रहेगी पर शान्ति और क्षमा के पीछे उनके रक्षार्थ वांछित शक्ति भी हो, शक्ति के बगैर अहिंसा कायरता और और दुर्गुण है। वीर और सामर्थ्यवान के लिए अहिंसा और क्षमा आभूषण हैं पर कायरों के लिए अर्थहीन है।
सत्य, धर्म, अहिंसा, करुणा,क्षमा,प्रेम और त्याग के लिए, बुद्ध और बुद्धत्व की रक्षा के लिए कृष्ण का होना अनिवार्य है।तथागत बुद्ध की जयन्ती पर उनको कोटिशः नमन । नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय।
--------
शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पांव : शक्ति आलेख : १ / ३ / ५ .
---------
पांचाली का तंज : चीरहरण : भीम की प्रतिज्ञा : और महाभारत :
*
आलेख : अरूण कुमार सिन्हा.
शक्ति.आरती.
*
आलेख :संदर्भित. लघु फिल्म : साभार : द्रौपदी : चीर हरण : शब्द : महाभारत
*
शब्द संभारे बोलिए : आघात शब्द बोलते लिखते सुनते या पढ़ते ही एक बात तो साफ हो जाती है कि आघात के दो स्वरुप होते हैं, भौतिक और अभौतिक या सूक्ष्म,जिस आघात में अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग हों,हिंसक आघात है और जिस आघात में इनके प्रयोग न हों सूक्ष्म, अभौतिक या वैचारिक आघात है।अस्त्र शस्त्र के आघात से ज्यादा घातक सूक्ष्म या वैचारिक आघात होते हैं जो शरीर को तो आहत नहीं करते पर ज्यादा सांघातिक होते हैं जो मनुष्य के मन मस्तिष्क हृदय और आत्मा को गहराईयों में जाकर आहत कर देते हैं।बाहरी आघात के घाव कालान्तर में भर जाते हैं और धीरे-धीरे मिट भी जाते हैं परन्तु जो सूक्ष्म या वैचारिक आघात होते हैं, सबसे घातक होते हैं। वैचारिक आघात एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करता है जो मनुष्य को भीतर से छिलता रहता है।इस सन्दर्भ में सद्गुरु कबीर साहब ने सच ही कहा है कि,
शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पांव
एक शब्द कर औषधि एक शब्द कर घाव
प्रायश्चित और पश्चाताप : और यह घाव ऐसा होता है जो जीवनपर्यन्त सालता रहता है जिसका कोई निदान नहीं होता। और होता भी है तो सच्चे हृदय से किया गया प्रायश्चित और पश्चाताप पर फिर भी मनोमस्तिष्क के किसी कोने में वह सुशुप्तावस्था में पड़ा रहता है जो सुशुप्त ज्वालामुखी की तरह किसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फूटकर निकल भी सकता है।
आघात करना उतना गंभीर नहीं होता है जितना कि आघात करने या पहुँचाने के बीज और गुण-धर्म का होना, पल्लवित और पुष्पित होना कि एकाएक आप लाठी उठाकर किसी पर प्रहार नहीं कर सकते है। वह भाव * प्रच्छन्न रूप से आपके * मन हृदय और मस्तिष्क में कहीं न कहीं बीज रूप में दबा रहता है जो समय की अनुकूलता को पाकर जीवित हो उठता है और आघात का सृजन होता है।
अब आप कुछ प्रसंगों का अवलोकन करें जो एक जीवित दस्तावेज हैं।
पांचाली का तंज : अंधे का बेटा अंधा महाभारत के नवनिर्मित पाण्डवों के रंगमहल का शुभारंभ होना था, जिसमें अद्भुत वास्तुकला का प्रयोग किया गया था कि सतह जो सुखी हुयी थी, पानी से लबालब भरी नजर आती थी और सतह जिस पर पानी था,सुखी नजर आती थी। दूर्योधन गुजर रहा था, जहां पानी न हो वह अपनी धोती उठा लेता था और जहां पानी हो धोती छोड़ देता था। पांचाली छज्जे पर से सब देख रही थी,उसने अट्टहास करते हुए तंज कसा कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है।
चीरहरण : भीम की प्रतिज्ञा : और महाभारत : यह तंज दूर्योधन को भीतर तक शूल की तरह चूभ गया और उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह इस अपमान का बदला द्रौपदी से जरूर लेगा जिसकी परिणति उसके चीरहरण से हुयी जो महाभारत का कारण बना।यह वैचारिक या सूक्ष्म आघात का जीवन्त उदाहरण है।
हिटलर प्रथम विश्वयुद्ध में बातौर एक जर्मन सिपाही की तरह लड़ा था। वह नख शिख घायल होकर पड़ा था जिसे डॉक्टरों ने लगभग मृत घोषित कर दिया था, उसके कानों में यह घोषणा सुनाई पड़ी कि जर्मनी युद्ध में हार गया है और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने जर्मन प्रतिनिधियों को बुरी तरह अपमानित किया है तो यह आघात वह सह नहीं सका और वह चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हुआ कि जर्मन कौम एक स्वाभिमानी कौम है,वह कभी पराजित नहीं हो सकता और वह स्वस्थ हो गया और उसने नात्सी दल की स्थापना की और जर्मनी पर कब्जा कर लिया,यह वैचारिक आघात था जिसने संसार को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया। वैचारिक आघात बड़े विध्वंसक होते हैं जो बड़े वर्णपटों पर परिणाम को ला खड़ा करते हैं।
इसलिए निजी जिन्दगी से लेकर सामाजिक जीवन में इस आघात प्रतिघात से सदैव बचने की जरूरत है कि इसके परिणाम अधिकांशतः नाकारात्मक ही होते दिखाई दिए हैं।
स्तंभ : शक्ति.सम्पादिका. डॉ. नूतन
लेखिका. देहरादून : उत्तराखंड.
सज्जा : शक्ति मीडिया
-----------
गौतम बुद्ध : अंगुलीमाल : हम तो ठहर गए,भला तुम कब ठहरोगे ? शक्ति : आलेख :१ / ३ / ४ .
-------------
अरूण कुमार सिन्हा.
बीच जंगल में आवाज गूंजी : ' ठहरो, कौन है, विरान जंगल में एक कठोर और कर्कश आवाज गूंज उठी....,
एक शमित जवाब मिला कि, ' हम तो ठहर गए,भला तुम कब ठहरोगे ?
इस जवाब को सुनकर पहले बोलने वाला दंग रह गया कि उसकी आवाज सुनकर लोगों की घिग्घी बंध जाती थी,डर से लोग थर-थर कांपनें लगते थे।
भला यह कौन है जो जवाब दे रहा है। वह बिहडों से निकलकर बाहर आया। बड़ी-बड़ी लाल लाल आंखें, भयानक डरावना चेहरा, गले में मानव अंगुलियों की माला और खून सनी तलवार लिए वह सामने खड़े आदमी को देख रहा था जो अपने हाथों में भिक्षा पात्र लिए, संन्यासी वेशभूषा वाला, दैदीप्यमान चेहरा वाला एक व्यक्ति सामने खड़ा था जिसके तेज से वातावरण में एक अजीब सी आभा फैल रही थी।
हिंसक डकैत जो अंगुलीमाल था,उसने बड़े शान्त स्वर में पुछा, हे महानुभाव,आप कौन हैं और इस विरान जंगल में क्या कर रहे हैं, संन्यासी जो तथागत सिद्धार्थ थे, उन्होंने बड़े शान्त स्वर में जवाब दिया कि,
मैं तो समझ गया हूॅं कि मैं कौन हूॅं और इसलिए मैं ठहर गया पर तुम कब ठहरोगे।
अंगुलीमाल समझ नहीं पाया कि इसका क्या जवाब दें,उसने कहा कि, हे संन्यासी कहीं आप गौतम बुद्ध तो नहीं हैं कि राजा प्रसेनजीत तक हमसे भयाक्रांत रहते हैं,उनके सेनापति और सेना भी हमसे डरती है और ऐसा निर्भय तो गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। हमने आपके बारे में सुना था,आज साक्षात्कार भी हो गया। अब आप ही बताएं कि आपके ठहरने और हमारे ठहरने का क्या अभिप्राय है,इसे स्पष्ट करने की कृपा करें।
तब तथागत सिद्धार्थ ने कहा,
आप शान्त भाव से बैठकर हमारी बातों को सुनें। अंगुलीमाल अपने कटार को जमीन पर रखकर घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गया।
बुद्ध ने कहा, हम भी ऐसे ही गतिशील थे और सुखभोग में लीन थे, कपिलवस्तु के राज्य का अधिपति था,किसी भी सुख वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं थी पर हम जब ठहर गए अर्थात् जीवन के निस्सारता को समझ गए तो परिव्राजक हो गए और ठहरी हुई अवस्था में चैतन्य हो गए और उसके बाद मैं गतिशील हो गया कि आप जैसे लोगों को ठहरा कर जीवन के यथार्थ को समझा सकुं।
हम सब किसके लिए सुकर्म या अपकर्म करते रहते हैं,इसके जिम्मेदार कौन होते हैं। हमारे कर्म हमारे होते हैं, कर्मजनित संस्कारों के प्रतिफल को कर्ता होने के कारण हमें ही भोगना पड़ता है और यही भोग जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ साथ चलते रहता है और जबतक वे संस्कार जीवित रहते हैं, हमें भोग से मुक्ति नहीं मिलती और यही पुनर्जन्म के कारण बनते हैं जिनसे हमारा प्रारब्ध बनता है। इसलिए हे अंगुलीमाल,अब ठहर जाओ और शेष जीवन को परिष्कृत और मर्यादित करने की कोशिश करो और इस जीवन की त्रासदी से मुक्त हो जाओ कि तुम ही तुम्हारे कर्मों के भोक्ता हो।
अंगुलीमाल रोने लगा, हे महात्मना,अब आप हमें मुक्ति मार्ग बताकर मुक्त करने की कृपा करें। बुद्ध ने उसे दीक्षित करके भिक्षु समूह में शामिल कर लिया और कालान्तर में वह सिद्ध संन्यासी हो गया।
अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इस कथा को सुनाने का क्या औचित्य है, हम तो कोई हिंसा या लूटमार नहीं कर रहे हैं तो हमें ठहरने की या अंगुलीमाल की तरह विलाप करने या पश्चाताप आदि करने की क्या जरूरत है।
स्तंभ संपादन
शक्ति.सम्पादिका. डॉ. नूतन
लेखिका. देहरादून : उत्तराखंड.
हिंसा का अर्थ सिर्फ खून-खराबा नहीं होता है, १ / ३ / ३ .
अमर्यादित शब्दों से किसी के अंतर मन को आहत करना भी हिंसा ही है
सवाल वाजिब है पर आपको इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है कि हिंसा का अर्थ सिर्फ खून-खराबा नहीं होता है, लूटपाट का मतलब सिर्फ लोगों को लूटना ही नहीं होता है। हिंसा बहुआयामी कृत्य है। हम सब रोज हिंसा करते रहते हैं कि हिंसात्मक क्रियाशीलता स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के होते हैं,एक तो मार पीट कर किसी को आहत करना या हत्या कर देना जिसके लिए वैधानिक कानून की व्यवस्था है और आपको इसके लिए वाजिब दण्ड भी दिया जाता है परन्तु उससे भी बड़े वर्णपट पर सूक्ष्म हिंसा का स्वरूप है जिसका गंभीरता से अवलोकन करने की जरूरत है।
क्षमापर्व की अवधारणा : भगवान महावीर ने इसीलिए खम्मन परब अर्थात् क्षमापर्व की अवधारणा को जन्म दिया कि हमें एकबार जड़ चेतन सबसे क्षमा मांगनी चाहिए कि जाने अनजाने में हम सब ऐसी भूल करते रहते हैं।
अब आप अपने निजी पारिवारिक और सामाजिक जीवन में समस्त क्रियाशीलताओं का अवलोकन और विश्लेषण करें कि चौबीस घंटों में आपने किसके साथ क्या बोला, क्या व्यवहार और आचरण किया तो आपको हिंसा का स्वरूप समझ में आ जाएगा। आपने अपनी पत्नी, बच्चों और मित्रों के साथ क्या व्यवहार किया,कितने झूठ बोले, कितनों के साथ दुर्व्यवहार किया आदि सभी हिंसा के ही रुप हैं।
आप परिवार में समर्थ हैं, समाज में ताकतवर हैं,पदबल, भुजबल से समर्थ हैं,लोग आपके भय से कुछ नहीं बोलते पर भीतर से उनका मन उनका हृदय और आत्मा आहत होती होगी,आह निकलती होगी और इसका प्रतिफल आपको ही भोगना होगा कि आप ही कर्ता है तो आपको ही भोक्ता होना होगा,
इसलिए तथागत सिद्धार्थ ने अंगुलीमाल को सम्बोधित करते हुए सबको कहा कि हम तो ठहर गए,भला तुम कब ठहरोगे।सवाल हम सबके सामने है और जवाब हम सबको ही देना है। देर सबेर सबको ठहरना होगा कि ठहरने का कोई विकल्प नहीं है।
अति से, हिंसा से, झूठ फरेब आदि से बचिए कि यही ठहरना है,महत्तम प्रयास करें कि आपके व्यवहार आचरण आदि से किसी का मन हृदय और आत्मा आहत न हो,यही हिंसा है, सिर्फ मार-पीट ही हिंसा नहीं है। सबके पास इतना समय जरूर शेष रहता है कि वह ठहर जाए और ठहर कर अपने को रुपान्तरित कर लें ।
--------
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम :सर्वयुग पुरुष : आलेख : १ / ३ /१ .
------------
अरूण कुमार सिन्हा.
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम : आज भगवान श्री राम की जयन्ती है जिसे वैश्विक स्तर पर इनके भक्त, श्रद्धावान और अनुगामी एक उत्सव, त्योहार और पर्व के रुप में मनाते हैं। श्री राम सिर्फ एक युग के ही महापुरुष और विभूति नहीं थे, अवतारी ही नहीं थे बल्कि अपने कृत्यों से अकाल पुरुष, सर्वयुग पुरुष,सार्वकालिक और सार्वभौमिक बन गए। उन्होंने समस्त समाज और आधारभूत संरचनाओं के लिए जिन मान्यताओं और मापदण्डों की स्थापना की,उनसे वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। वे अवतारी होने के कारण या हिन्दू समाज के आराध्य होने के कारण नहीं बल्कि हर पारिवारिक और सामाजिक मान्यताओं के पालन और स्थापना करने के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन सके।
जयन्ती मनाने के पीछे महती उद्देश्य : आज सिर्फ एशियाई देशों में ही नहीं वरन् वैश्विक स्तर इनकी आराधना साधना और पूजा की जाती है। यहां यह उल्लेखनीय हो जाता है कि आखिर जयन्ती मनाने के पीछे महती उद्देश्य क्या है, जयन्ती मनाने के पीछे वैश्विक समाज को स्मारित कराना होता है कि आज मानव समाज में जो इतनी विकृतियां आयी हैं, रिश्ते अमर्यादित हुए हैं, चहुंओर हिंसा, रक्तपात, शोषण दोहन आदि जो बढ़े हैं उनके पीछे एक ही कारण है कि हमारा समाज स्थापित मर्यादाओं के मापदण्डों को विस्मृत कर गया है। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की मर्यादा नष्टप्राय हो चुकी है, इसलिए आज वैश्विक स्तर शत्रुओं के साथ भी मर्यादित व्यवहार : आज भगवान श्री राम की उपयोगिता, उपादेयता और प्रासंगिकता है। माता-पिता, भाई, पत्नी, मित्र, सहयोगी, गुरु,सेवक, भक्त,साधक,आराधक यहां तक कि शत्रुओं के साथ भी उन्होंने मर्यादित व्यवहार किया जिनके सम्मान, पुनर्मूल्यांकन और अनुपालन की आज भी जरूरत है और कल भी रहेगी।
सत्य वही है जो शाश्वत और सनातन है, जिसके गुणधर्म अपरिवर्तनशील हैं, सार्वभौमिक और सार्वकालिक है और ऐसी ही मर्यादा भगवान श्री राम की है जो किसी मत,पंथ, विश्वास, विचार, सिद्धान्त, सम्प्रदाय आदि से बंधा नहीं बल्कि समस्त मानव समुदाय के लिए प्रासंगिक और उपयोगी है, जिसके सहज और सरल अवलोकन की जरूरत है और समाज को हर अपराध, प्रदूषण, अत्याचार, अनाचार, अपराध आदि से सुरक्षित करने के लिए सबको श्री राम को समझने और अपनाने की जरूरत है,जैसे नीति शास्त्र और आचार शास्त्र होते हैं वैसे ही श्री राम व्यवहार और आचरण हैं जिनका अनुसरण करना जीवन के मोल और मूल्य हैं जिन्हें किसी मत,पंथ, विश्वास, विचार, सम्प्रदाय आदि के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए जैसे डाक्टर की जाति और मत आदि हो सकते हैं पर औषधि की कोई जाति,मत,पंथ आदि नहीं होते वही औषधि श्री राम हैं। समस्त मानव समाज को श्री राम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाईयां एवं मंगलकामनाऍं
-------
श्री कृष्ण के दर्शन से ज्यादा सुन्दर क्या होगा : ? रुक्मिणी राधा मीरा आलेख : १ / ३ /०.
---------
अरूण कुमार सिन्हा.
श्री कृष्ण के दर्शन से ज्यादा सुन्दर क्या होगा : रुक्मिणी. राधा. मीरा. : कोई रुक्मिणी, राधा , मीरा और गोपियों से पुछे कि सौन्दर्य क्या है ? सब जानते है उनका जवाब क्या होगा ? कोई मीरा, रसखान ,बिहारी या सूरदास से पुछे कि सौन्दर्य क्या है,तो एक ही जवाब होगा,श्री कृष्ण के दर्शन से ज्यादा सुन्दर क्या होगा ? कोई हनुमान जी से पुछे कि इस ब्रह्माण्ड में सबसे सुन्दर क्या है तो जवाब होगा श्री राम,इस तरह सौन्दर्य तो एक ही है जो समस्त पदार्थों में समाहित है पर नजरें तो अनन्त हैं इसलिए सौन्दर्य के स्वरूप बदल जाते हैं, पर सेनेका कहता है कि इस दुनिया में खुबसूरत नजारों की कमी नहीं है परन्तु सबसे खूबसूरत नजारा किसी आदमी को एकदम विपरीत परिस्थितियों में न हार मानते हुए जूझते हुए देखना है,आप इससे कितना सहमत हैं।
कृष्ण के दर्शन व उनके व्यक्तित्व में अटूट विश्वास रखने वाले अनन्य भक्त भी कहते है ,
'हे माधव ! यदि आप मेरे जीवन के सारथी हो जाए तो मैं किसी ऐसे नूतन विश्व का निर्माण कर ही लूंगा
जिसमें मात्र अनंत ( श्री लक्ष्मीनारायण ) शिव ( कल्याणकारी ) शक्तियाँ ही होगी
होलिका की अग्नि में मेरे अंतर्मन की चिर ईर्ष्या, पीड़ा ,द्वेष ,और बुराई जलकर भस्म हो.....
हे : परमेश्वर : आदि शक्ति : जीवन के इस अंतहीन सफ़र में तू मुझे मात्र ' सम्यक साथ ' प्रदान कर जिससे मेरी ' दृष्टि ' , ' सोच ' ,' वाणी ', और ' कर्म ' परमार्जित हो सके...'
जिन्दगी एक अनवरत संघर्षों की गाथा है : हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि जितनी नजरें उतनी खुबसूरती नजर आती है। पर जिन्दगी जो एक अनवरत संघर्षों की गाथा है जिसमें कोई संसाधनपूर्णता में संघर्ष करता है तो कोई संसाधनहीनता में भी संघर्ष करता नजर आता है। कविवर निराला जी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती, संघर्ष करती औरत में जो सौन्दर्य नजर आता है,वह अप्रतिम सौन्दर्य है।
स्तंभ संपादन : सौन्दर्य और हमारी दृष्टि. : अलग अलग :
शक्ति.सम्पादिका. डॉ. नूतन
लेखिका. देहरादून : उत्तराखंड ---------
सत्य वह नहीं जो हम देखते हैं : सम्पादकीय : आलेख :.
----------
सत्य वह नहीं : मनन चिन्तन और विश्लेषण की आवश्यकता : सत्य वह नहीं जो हम पढ़ते,लिखते, सुनते या बोलते हैं क्योंकि सत्य तो वही है जो सबके लिए ग्राह्य हो और जिसका बोध निरपेक्ष हो।
हर व्यक्ति अपने भोगे हुए यथार्थ, पढ़े हुए विषय,देखे हुए दृश्य और सुने हुए विषय को ही समझता है जो प्रायः सापेक्ष ही होता है तब आप कैसे समझेंगे कि यही सत्य है तो आपको उन तथ्यों का मनन चिन्तन और विश्लेषण करना होगा और उनकी तह तक जाना होगा और तभी आप सत्य को जान पाएंगे।
कोई व्यक्ति यह कह दे कि मैंने मीठा करैला खाया है, कोई कह दे कि मैंने जो गन्ना खाया वह खट्टा था। आपको सहज ही विस्मय होगा कि करैला न तो मीठा हो सकता है और न गन्ना खट्टा हो सकता है चूंकि आपने भी उनके स्वाद चखे हैं और आपको भी उनके स्वाद की पूर्वानुभूति रही है तो दूसरे ने कहा और आपने भी सहमति दी, निस्संदेह वह सत्य है।
इस तरह कोई कथन, कोई दृश्य, कोई श्रव्य कथन सिर्फ पहले पर निर्भर नहीं करता बल्कि आपका साक्षात्कार जब उसे अन्दर से स्वीकार कर लेता है और उसके समर्थन में अन्य साक्ष्य भी होते हैं तो उसका भाव सापेक्ष से निरपेक्ष हो जाता है।
सत्य का स्वरूप : निर्विरोध निर्विवाद सार्वभौमिक और सार्वकालिक : सत्य का स्वरूप निर्विरोध निर्विवाद सार्वभौमिक और सार्वकालिक होता है और जिनमें ये विशिष्टताएं नहीं होती वह निरपेक्ष सत्य नहीं होता। संसार के समस्त मत,पंथ, विश्वास, विचार , सम्प्रदाय आदि और उनके नीति शास्त्र इससे सहमत हैं कि मनुष्य का जन्म सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए हुआ है। मनुष्य को सबके हित और मंगल की कामना करनी चाहिए,यह सत्य है।*
-------
सौन्दर्य और हमारी दृष्टि. : अलग अलग : : सम्पादकीय : आलेख :
--------
सौन्दर्य और हमारी दृष्टि : अलग अलग : इस ब्रह्माण्ड में सौन्दर्य की कोई कमी नहीं, सर्वत्र सुन्दरता बिखरी हुयी है पर सबके अवलोकन के दृष्टिकोण अलग-अलग होते हैं। जिस व्यक्ति के जो भाव विचार होते हैं उसी दृष्टिकोण से वह सौन्दर्य की तलाश करता है। किसी को सुन्दर पुरुष या स्त्री में सौन्दर्य नजर आता है तो किसी को खुबसूरत फूल या प्राकृतिक आधारभूत संरचनाओं में सौन्दर्य नजर आता है आता है तो किसी को सुन्दर भवन आकर्षित करता है।
कोई सुन्दर गीत संगीत को सुनकर भाव विभोर हो जाता है तो कोई सुन्दर साहित्य,लेखन, मूर्ति कला, वास्तुकला, संभाषण आदि में सौन्दर्य की तलाश करता है और अपने दृष्टिकोण से उसे पाकर खुश हो जाता है, संगीत के बारे में तो कहा भी गया है कि जो हृदय संगीत की लहरों से विचलित न हो वह आदमी हृदय विहीन होता है,वह आदमी हो ही नहीं सकता है।
--------
भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए : सम्पादकीय : पद्य संग्रह : पृष्ठ : २ / २ .
--------
अरूण कुमार सिन्हा.
शक्ति.आरती
*
लघु कविता
*
प्रेम तू क्या है
कृष्ण को राधा और राधा
को कृष्ण
*
प्रेम
ओ प्रेम !
तु तो एक तिलस्म है
करिश्मा है प्रेम !
तु तो अनंग होते हुए
भी वह कर सकता है कि
चेतना बुद्धि विवेक सब
मिलकर भी नहीं कर सकते
दो को एक करने का हुनर
तो तुम्हारे ही पास है
कृष्ण को राधा और राधा
को कृष्ण तो तु ही
बना सकता है
एक रानी को मीरा
तु ही बना सकता है
निर्गुण ( उद्धव जी ) को सगुण
भी तु ही बना सकता है
कहते हैं प्रेम न तो लेन देन है
न नफा नुकसान है
ना ही कोई विवशता
या व्यवसाय है
प्रेम न तो याचना है
ना कोई इच्छा या कामना है
यह तो मुक्त है स्वतंत्र है
निर्वाण है कैवल्य है ,मोक्ष है
संसार चक्र से मुक्ति का
एकमात्र मार्ग है, प्रेम
ओ प्रेम, तु तो गुंगे का गुड़ है
कबीर के तलवार की म्यान है
राम की मर्यादा कृष्ण का आनन्द है
जीण का क्षमा
तथागत की करूणा है
जीसस का प्रेम
मोहम्मद का तौहिद है ,प्रेम
तु संतों की गुरूवाणी भी है
तुम्हारी कोई जाति धर्म
रंग रूप भी नहीं है
कोई भाषा भी नहीं है
पर प्रेम की भाषा से बड़ी
कोई भाषा भी नहीं है
जिसे पढ़ने समझने के लिए किसी इल्म की
जरूरत नहीं है
बस एक अदद दिल की
जरूरत होती है
जिसे कभी राम ने भी जानकी
विरह में पढ़ा
जिसे भगवान चैतन्य ने पढ़ा
जिसे मंसूर और सरमद ने पढ़ा
मन और दिमाग से इसका क्या
वास्ता
प्रेम तु तो अनहद नाद है
ब्रह्माण्ड का शून्य है और जो
शून्य है
वही तो शिव है
शिव ही सत्य है सौन्दर्य है
प्रेम
तु ही तो सत्यम् शिवम् सुन्दरम्
का अजस्र मार्ग है
प्रेम
ओ प्रेम
अंत में तु तो अज्ञेय है।।
*
पृष्ठ सज्जा : महाशक्ति मीडिया.
स्तंभ संपादन : शक्ति.शालिनी क्षमा कौल . कवयित्री लेखिका. जम्मू
*











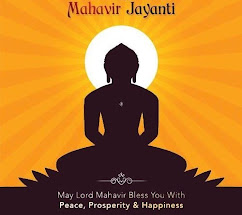
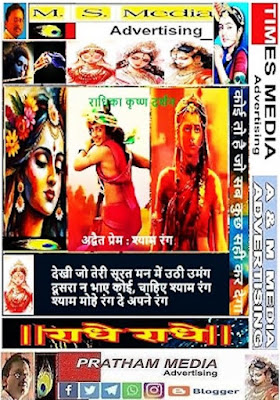


Comments
Post a Comment